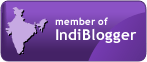इस समय पूरा विश्व कोरोना-जनित महामारी की चपेट में है। कोरोना नामक विषाणु चीन के वुहान शहर से निकलकर सर्वत्र फैल चुका है। खुद चीन में यह कहां से आया यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि वुहान में चमगादड़ों के साथ-साथ अन्य पशु-पक्षियों का मांस बिकता है और विषाणु वहां के चमगादड़-मांस से लोगों के बीच फैला। कुछ लोगों का कहना है कि वुहान की एक विषाणु प्रयोगशाला में ही कोरोना का जन्म हुआ और किसी चूक से यह बाहर नगरवासियों में फैल गया। एक मत यह भी है कि आर्थिक तौर पर दुनिया को पंगु करने के लिए चीन ने इसे ईजाद किया और दुनिया में फैलने दिया। ऐसे अनेक मत व्यक्त किए जा सकते हैं। वास्तविकता क्या है यह अभी कोई नहीं जानता। बस इतना सच है कि इस विषाणु ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को रोगग्रस्त कर दिया है और लाखों को काल के गाल में पहुंचा दिया है।
कोरोना के महाप्रकोप को रोकने का कोई कारगर उपाय किसी के पास नहीं है। न ही रोगग्रस्त लोगों के लिए कोई प्रभावी इलाज अभी तक मिल सका है। ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुनिया की विभिन्न सरकारों ने “लॉकडाउन” का सहारा लिया है। यह ऐसा शब्द है जिसका इतना व्यापक प्रयोग पहले कभी सुना नहीं गया था। लॉकडाउन ने खुद अपने किस्म की समस्याएं पैदा कर दी हैं। पूरी सामाजिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गयी है। आर्थिक क्रियाकलाप रुक गये हैं और अधिकांश लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गये। सबसे विकट समस्या उन लोगों के सामने है जो घर-परिवार से दूर जहां थे वहीं फंस के रह गये हैं।
अपने देश में लॉकडाउन से कोरोना के प्रसार पर संतोषप्रद नियंत्रण मिल सका तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि तथा राहत की चीज होगी। लॉकडाउन की जो कीमत चुकानी पड़ रही है उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, विवशता में ही सही। फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि कोरोना ने लॉकडाउन की आवश्यकता को जन्म दिया और लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी को अप्रत्याशित कष्ट में धकेल दिया।
लेकिन इस लॉकडाउन के कुछएक सकारत्मक पहलू भी देखने को मिल रहे हैं। जो लोग घरों में अधिक टिक नहीं सकते थे, उन्होंने घर में टिकना और परिवारी जनों के साथ समय बिताना सीख लिया। लोगों में एक प्रकार की उपकारिता की भावना भी जागृत हुई है। पुलिसबल का व्यवहार काफी कुछ बदला नजर आने लगा है। अधिकांश जन कोरोना से लड़ाई के प्रति योगदान देने को प्रेरित भी हो रहे हैं। ये सब संतोष की बातें है। आगे के सामय में ये बातें कुछ हद तक स्थायित्व भी पा सकती हैं।
इस कोरोना-संक्रमण काल में कुछ लोग बहुत-से वे कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। इसी क्रम में मुझे अपने एक मित्र की दैनिक चर्या में विवशता-जनित परिवर्तन के बारे में सुनने को मिला। इस समय मैं स्वयं अपने घर से दूर अन्य शहर में अटका हुआ हूं। मैंने कई बार उनसे फोन पर बात करने और हालचाल पूछने का प्रयास किया। लेकिन संपर्क साधने में सफल नहीं हुआ। अन्य मित्रों एवं परिचितों से उनकी कुशलक्षेम की जानकारी मुझे मिल गई। मुझे पता चला कि वे चाय-नाश्ता और भोजन-सामग्री बनाना सीख रहे हैं। यह समाचार मेरे लिए रोचक एवं अविश्वनीय था। क्यों, बताता हूं।
मेरे मित्र महोदय उम्र में सत्तर-प्लस हैं। सेवानिवृत्त हैं और अकेले रहते हैं। परिवार में कोई और उनके साथ नहीं रहता। इसलिए उन्होंने लगभग सभी दैनिक कार्यों के लिए परिचारक-परिचारिकाओं यानी घरेलू सहायक का सहयोग लिया है। ये सहायक सुबह-शाम का नाश्ता, दोपहर-रात्रि का भोजन, घर का झाड़ू-पोछा, लत्ते-कपड़ों की धुलाई, आदि लगभग सभी कार्य करते हैं। निर्धारित समय पर आते हैं, अपने-अपने हिस्से का कार्य निपटाते हैं, और लौट जाते हैं। इसलिए मित्र महोदय को कोई काम नहीं करना पड़्ता है। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। अभी तक उनके कार्य सुचारु रूप से चल रहे थे।
लेकिन इस बार लॉकडाउन ने उनके सामने गंभीर समस्या पैदा कर दी है। चूंकि लोगों को यथासंभव घर तक सीमित रहना है, और केवल जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने की छूट मिल पा रही है मगर वह अधिक देर के लिए नहीं। इसलिए उनके घरेलू सहायकों का आना-जाना बंद हो गया। चाय कौन बनाए, भोजन कैसे बनेगा, झाड़ू भी लग पायेगा क्या, गंदे कपड़ों का क्या होगा, आदि प्रश्न उनके सामने उठ खड़े हो गये। ऐसे मौकों पर आदमी अपनी झल्लाहट या गुस्सा किसी न किसी पर उतारना तो चाहेगा ही। सामने कोई हो तो उसी को दो-चार बातें सुना दे लेकिन उनके घर में कोई और हो तब न? जिसने इस लॉकडाउन का निर्णय लिया उसी पर उन्होंने कल्पना में गुस्सा उतार दिया। कर भी क्या सकते हैं?
पिछले कई वर्षों से वे घरेलू सहायकों पर ही निर्भर रहे इसलिए चाय बनाना भी अब बेहद मुश्किल का काम लग रहा था। करते क्या? शनैः-शनैः चाय-नाश्ता-भोजन बनाना शुरू कर दिया, जैसा भी बन पड़ा। पिछली बार परिचितों-मित्रों से इतना तो मुझे खबर मिली। झाड़ू-पोछा करना और कपड़े धोना अभी शुरू हुआ कि नहीं पता नहीं चला। ये दोनों कुछ दिन टल सकते हैं लेकिन भोजन-पानी नहीं। मोबाइल फोन पर मुझे उत्तर मिलता नहीं। सोचता हूं सब ठीक ही चल रहा होगा। – योगेन्द्र जोशी